रिट (Writ) क्या है?
रिट का अर्थ है “न्यायिक आदेश”।
जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है।
भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट्स (Writs)
- हबीयस कॉर्पस (Habeas Corpus)
- मैंडेटस (Mandamus)
- प्रोहिबिशन (Prohibition)
- सर्टियोरारी (Certiorari)
- क्वो वारंटो (Quo Warranto)
भारतीय संविधान की 5 रिट्स मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक आदेश के रूप में कार्य करती हैं। ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जारी की जाती हैं।
अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 का महत्व
अनुच्छेद 32
- यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है।
- इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट्स (Writs) जारी करने की शक्ति है।
अनुच्छेद 226
- यह राज्य उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए रिट्स जारी करने का अधिकार देता है।
- उच्च न्यायालय का अधिकारक्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है।
भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट्स (Writs) का प्रावधान है:
| रिट का नाम | हिंदी अर्थ | उद्देश्य |
|---|---|---|
| Habeas Corpus | “शरीर को पेश करो” | अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाना |
| Mandamus | “आदेश दो” | लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना |
| Prohibition | “रोक लगाने का आदेश” | निचली अदालत को गलत अधिकार प्रयोग करने से रोकना |
| Certiorari | “जांच करने का आदेश” | मामला उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना |
| Quo Warranto | “किस अधिकार से?” | किसी पद पर बैठे व्यक्ति की वैधता को चुनौती देना |
भारतीय संविधान के पाँचों रिट्स (Writs) का विस्तृत विवरण

1. Habeas Corpus – हबीयस कॉर्पस
अर्थ:
“तुम शरीर को प्रस्तुत करो” – यह लैटिन भाषा से लिया गया है।
यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो।
उद्देश्य:
- किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत से मुक्त कराना।
- यह सरकार, पुलिस या किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकती है।
मुख्य विशेषताएँ
- यह सरकार, पुलिस या निजी व्यक्ति – किसी के भी खिलाफ जारी की जा सकती है।
- कोर्ट उस व्यक्ति को सामने प्रस्तुत करने का आदेश देती है जिसे हिरासत में लिया गया है।
- इसके तहत कोर्ट यह जांचता है कि हिरासत कानूनी है या अवैध।
यदि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण या वारंट के गिरफ्तार कर लेती है, और उसका परिवार कोर्ट में याचिका दायर करता है, तो कोर्ट Habeas Corpus रिट जारी करके पुलिस से कहेगा:
“उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करो और बताओ कि उसे क्यों हिरासत में रखा गया है।”
नोट:–
- Habeas Corpus सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली रिट मानी जाती है।
- यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है।
- यह आपातकाल की स्थिति में भी अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है (44वां संशोधन, 1978 के बाद)।
2. Mandamus – मैंडेटस
अर्थ:
Mandamus एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है — “हम आदेश देते हैं” (We Command)
यह रिट सरकारी अधिकारियों या संस्थाओं को उनके कानूनी कर्तव्य का पालन कराने के लिए कोर्ट द्वारा जारी की जाती है।
उद्देश्य:
- सरकारी अधिकारी, संस्था या लोक निकाय को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देना।
- जब कोई लोक सेवक या अधिकारी अपने वैधानिक कार्यों को करने से मना करता है, तब यह रिट लागू होती है।
मुख्य विशेषताएँ
- केवल सरकारी निकाय, सरकारी अधिकारी, लोक सेवा आयोग, या सरकारी विश्वविद्यालय आदि पर लागू होती है।
- यह निजी संस्थानों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती।
- यह तब जारी की जाती है जब याचिकाकर्ता को कोई कानूनी अधिकार (legal right) प्राप्त हो और संबंधित संस्था उसे अनदेखा कर रही हो।
यदि शिक्षा विभाग पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है, तो हाई कोर्ट मैंडेटस जारी कर उसे आदेश दे सकता है कि वह अपना कर्तव्य निभाए।
नोट:–
- Mandamus रिट प्रशासनिक निष्क्रियता के विरुद्ध प्रभावी उपाय है।
- यह रिट तभी दी जाती है जब:
- संबंधित संस्था सरकारी हो, और
- याचिकाकर्ता का अधिकार कानून में स्पष्ट हो।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ यह रिट जारी नहीं की जा सकती (अनुच्छेद 361)।
- यह निजी संस्थाओं पर लागू नहीं होती।
3. Prohibition – प्रोहिबिशन (रोक आदेश)
अर्थ:
Prohibition का अर्थ है — “रोक लगाने का आदेश” (To Forbid/To Prohibit)
यह लैटिन शब्द से लिया गया है और तब उपयोग होती है जब कोई निचली अदालत या न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो।
उद्देश्य:
- किसी अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Court) को उसके क्षेत्राधिकार (jurisdiction) से बाहर जाकर कार्य करने से रोकना।
- यह सुनिश्चित करना कि अदालतें कानून के अनुसार ही कार्य करें।
- उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालतों को आदेश दिया जाता है कि वे मामले की सुनवाई न करें।
मुख्य विशेषताएँ
- यह रिट Supreme Court या High Court द्वारा निचली अदालतों या न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है।
- इसका उद्देश्य “कार्यवाही से रोकना” होता है — यानी मामला अभी जारी है, लेकिन उच्च न्यायालय आदेश देता है कि आगे की सुनवाई न की जाए।
- यह रिट अदालती या न्यायिक कार्य में अधिकार-सीमा का उल्लंघन रोकने के लिए होती है।
अगर कोई जिला न्यायालय ऐसा मामला सुन रहा है जो सिर्फ उच्च न्यायालय ही सुन सकता है, तो उच्च न्यायालय Prohibition रिट द्वारा उसे कार्यवाही से रोक सकता है।
नोट:–
- यह रिट कार्यवाही के दौरान ही जारी की जाती है (जब मामला समाप्त नहीं हुआ हो)।
- यह केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकायों पर लागू होती है — प्रशासनिक संस्थाओं पर नहीं।
- Prohibition रिट पूर्व-रक्षात्मक (preventive) होती है, जबकि Certiorari रिट बाद में सुधारात्मक (corrective) होती है।
- यह प्रशासनिक अधिकारियों या निजी संस्थाओं पर लागू नहीं होती।
- अगर कार्यवाही पहले ही पूरी हो चुकी हो, तो Prohibition लागू नहीं होती — उस स्थिति में Certiorari रिट दी जाती है।
4. Certiorari – सर्टियोरारी (स्थानांतरण आदेश)
अर्थ:
Certiorari एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है — “जानने के लिए” या “जांचने के लिए बुलाना” (To be certified or to inform)।
इसका उपयोग तब होता है जब कोई निचली अदालत या न्यायिक संस्था कानून का उल्लंघन कर चुकी हो या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय ले चुकी हो।
उद्देश्य:
- जब कोई निचली अदालत ग़लत तरीके से न्यायिक कार्य कर रही हो (बिना अधिकार या प्रक्रिया का उल्लंघन करके),
तब उच्च न्यायालय उस आदेश को निरस्त कर सकता है और मामला अपने पास मंगा सकता है। - यह रिट तब दी जाती है जब कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो, और उसमें कानून की गलती हुई हो।
मुख्य विशेषताएँ
- यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है, जब कोई निचली अदालत:
- अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चली गई हो।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया हो।
- कोई ऐसा निर्णय लिया हो जो कानून के विरुद्ध हो।
- यह रिट कार्यवाही पूरी होने के बाद जारी की जाती है (यानि Corrective in nature)।
यदि कोई जिला न्यायालय किसी व्यक्ति को बिना उचित सुनवाई के दोषी ठहरा देता है, या ऐसी कार्यवाही करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, तो हाई कोर्ट Certiorari रिट जारी कर उस निर्णय को रद्द कर सकता है।
नोट:–
- Prohibition और Certiorari दोनों रिट्स न्यायालयों के विरुद्ध होती हैं: Prohibition = कार्यवाही रोकने के लिए (मामला अभी जारी है) और Certiorari = निर्णय रद्द करने के लिए (मामला पूरा हो चुका है)
- Certiorari रिट एक सुधारात्मक (Corrective) उपाय है।
- प्रशासनिक निर्णयों पर (जब तक वो न्यायिक स्वभाव के न हों)
- निजी संस्थानों पर नहीं लागू होती
- यह रिट केवल अधीनस्थ न्यायिक निकायों पर लागू होती है
5. Quo Warranto – क्वो वारंटो (अधिकार का प्रश्न)
अर्थ:
Quo Warranto एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है — “किस अधिकार से?” (By what authority?)
यह रिट तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद (Public Office) पर अवैध रूप से काबिज हो।
उद्देश्य:
- यदि कोई व्यक्ति ग़लत तरीके से किसी सरकारी पद पर आसीन है, तो कोर्ट उसे पद छोड़ने का आदेश दे सकता है।
- यह रिट जनहित में होती है — किसी भी नागरिक द्वारा दायर की जा सकती है।
अगर कोई व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता या चयन प्रक्रिया को पूरा किए बिना किसी राज्य सरकारी पद पर नियुक्त हो गया है, तो कोई भी नागरिक Quo Warranto याचिका दायर कर सकता है।
कोर्ट आदेश देगा कि व्यक्ति उस पद को छोड़ दे।
मुख्य विशेषताएँ:
- यह रिट सार्वजनिक हित (Public Interest) में दायर की जाती है।
- इसे कोई भी नागरिक अदालत में दायर कर सकता है, भले ही उसका निजी हित प्रभावित न हो।
- यदि अदालत को लगता है कि व्यक्ति अवैध रूप से पद पर काबिज है, तो वह उसे पद खाली करने का आदेश दे सकती है।
नोट:–
- Quo Warranto रिट का उद्देश्य जनहित की रक्षा करना है — यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक पदों पर केवल योग्य और वैध लोग ही बैठे हों।
- यह रिट दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को उस पद पर स्वयं दावा करने की ज़रूरत नहीं होती।
- निजी पदों पर लागू नहीं होती (जैसे: निजी कंपनी के CEO)
- पद सरकारी और वैधानिक होना चाहिए
- नियुक्ति में कोई कानून का उल्लंघन होना चाहिए
| क्रम | रिट | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 1 | Habeas Corpus | अवैध हिरासत से मुक्ति |
| 2 | Mandamus | अधिकारी को उसका कार्य करने का आदेश |
| 3 | Prohibition | निचली अदालत को रोकना |
| 4 | Certiorari | आदेश रद्द कर मामला मंगवाना |
| 5 | Quo Warranto | किसी व्यक्ति से सार्वजनिक पद का अधिकार पूछना |

भारतीय संविधान के सभी पाँच रिट्स (Writs) का सारांश:
| रिट | उद्देश्य | लागू कहाँ होता है |
|---|---|---|
| Habeas Corpus | अवैध हिरासत से मुक्ति | किसी भी व्यक्ति पर (सरकारी या निजी) |
| Mandamus | कर्तव्य पालन का आदेश | सरकारी अधिकारी/संस्था पर |
| Prohibition | निचली अदालत को कार्य से रोकना | निचली अदालत या न्यायिक संस्था |
| Certiorari | निचली अदालत के निर्णय को रद्द करना | निचली अदालत या न्यायिक संस्था |
| Quo Warranto | अवैध पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना | सार्वजनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति पर |
- भारतीय संविधान में रिट्स की व्यवस्था नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रभावशाली माध्यम है।
- ये रिट्स विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है।
- सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) के पास यह विशेष अधिकार है कि वे किसी सरकारी अधिकारी, संस्था या न्यायिक निकाय के विरुद्ध रिट जारी कर सकें।
- इन पाँच रिट्स — Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto — के माध्यम से भारत में “न्याय सबके लिए” की संवैधानिक भावना को सशक्त किया गया है।
🔗 मौलिक अधिकारों पर लिंक:[भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को समझें]
अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान की अधिकारिक वेबसाइट देखें।
writs for UPSC in Hindi, writs notes in Hindi, writs summary for UPSC, writs important for mains

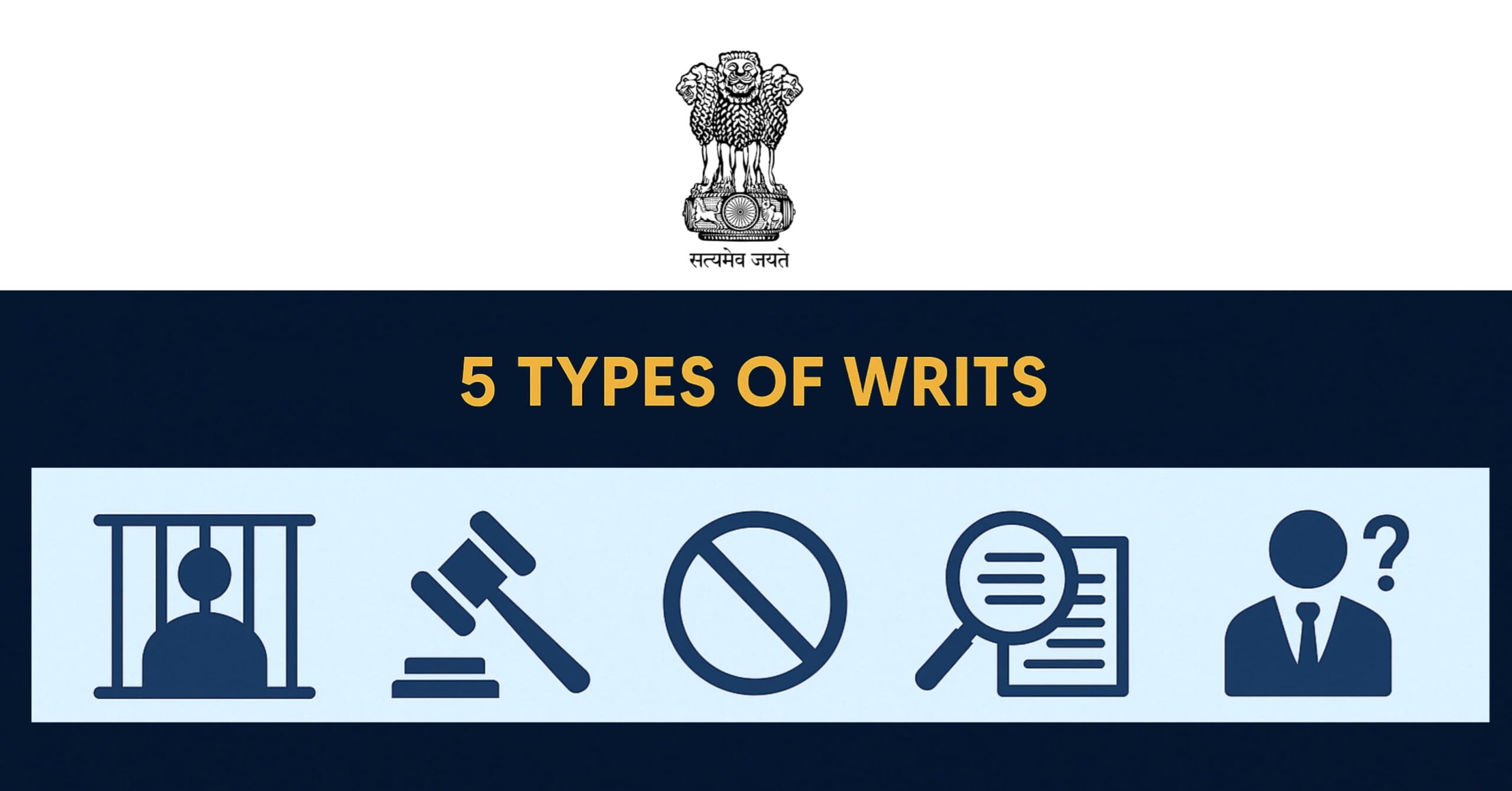
2 thoughts on “भारतीय संविधान की 5 रिट्स (Writs): अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएँ”